भारत के मध्यकालीन इतिहास में दो शासक अपने नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। एक थे सम्राट विक्र्माद्वित्तीय और दूसरे थे मुग़ल सम्राट अकबर। नवरत्न परम्परा के अनुसार,कोई भी योग्य व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र का महारथी हो उसको उस कार्य की जिम्मेबारी सौंप दो और खुद सत्ता का भोग करो।
आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इसी नियम पर अपने कर्मचारियों का चुनाव करती हैं। हालाँकि अभी तक राजनीति के महारथी इस बात को नहीं पकड़ पाए हैं।
Table of Contents
Toggleविक्र्माद्वितीय जिनके पास नवरत्न थे उनके समय को लेकर विद्वान एकमत नहीं हैं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि ये वो उज्जयिनी सम्राट विक्र्माद्वितीय थे जिनके नाम से विक्रम सम्वत चलता है इस प्रकार इनका समय 57 ईस्वी पूर्व से लेकर 19 ईस्वी के बीच में रहा होगा
परन्तु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये गुप्त वंश के महान शासक चन्द्रगुप्त विक्रमाद्वितीय थे जिनका कार्यकाल चौथी ईस्वी से लेकर पांचवी ईस्वी के बीच का बताया जाता है।
इतिहासकारों के मतभेद का कारण
इनके समय को लेकर मतभेद शायद इसलिए है क्यूंकि विक्र्माद्वित्तीय एक उपाधि थी जो भारतीय इतिहास में बहुत से राजाओं ने धारण की थी ये उपाधि वीरता, ज्ञान तथा न्याय का प्रतीक मानी जाती थी।
और दूसरा नवरत्नों के समय में भी मतभेद है जैसे कोई भी इतिहासकार इनके समय को लेकर स्पष्ट नहीं है अब नवरत्नों में से एक कालिदास को ही ले लीजिये। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम् नाटक लिखा जिसमे उन्होंने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक के रूप में चित्रित किया।
और अग्निमित्र का शासनकाल 170 ईसापू्र्व था इस प्रकार कालिदास का समय इससे पहले नहीं हो सकता। जबकि छठीं ईसवी में बाणभट्ट ने हर्षचरितम् लिखी उसमे कालिदास का उल्लेख किया है
और इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र मिलता है इस प्रकार वे इनके बाद के नहीं हो सकते। अत: कालिदास का समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसवी के बीच में कहीं रहा हो सकता है।
इसी प्रकार दूसरे नवरत्नों के समय में भी मतभेद है जैसे एक नवरत्न थे धन्वंतरि जो कि चिकित्सा विशेषज्ञ थे लेकिन प्राचीन समय में भारत में अनेक धन्वंतरि हुए हैं इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद प्राचीन समय में जो भी चिकित्सा विशेषज्ञ होता होगा उसे धन्वंतरि कहा जाता होगा।
इन सब मतभेदों के बावजूद ये नवरत्न थे ये तो तय है
सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्न कौन से थे
धन्वंतरि: ये एक महान चिकित्सक थे और आयुर्वेद के जानकार थे। इन्हे आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है।
क्षपणक: ये एक जैन मुनि थे और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे।
अमरसिंह: ये एक महान कोशकार थे और उन्होंने “अमरकोश” नामक संस्कृत शब्दकोश की रचना की।
शंकु: ये एक महान वास्तुकार थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया।
वेतालभट्ट: ये एक महान जादूगर थे और अपनी रहस्यमयी विद्याओं के लिए प्रसिद्ध थे।
घटखर्पर: ये एक महान कवि थे और उन्होंने कई सुंदर काव्यों की रचना की।
कालिदास: ये एक महान कवि और नाटककार थे और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्होंने “अभिज्ञानशाकुन्तलम्” और “मेघदूतम्” जैसे प्रसिद्ध काव्यों की रचना की।
वराहमिहिर: ये एक महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे और उन्होंने “पंचसिद्धान्तिका” नामक ग्रंथ की रचना की।
वररुचि: ये एक महान व्याकरणशास्त्री थे और उन्होंने “प्राकृतप्रकाश” नामक ग्रंथ की रचना की।
अकबर के 9 रत्नों के नाम क्या थे
मुग़ल सम्राट अकबर ने भी सम्राट विक्र्मद्वित्तीय की तरह नवरत्न की परम्परा अपनाई इसलिए इनका शासन मुग़ल समय का सबसे स्थापित और शांतिपूर्ण शासन माना जाता है।
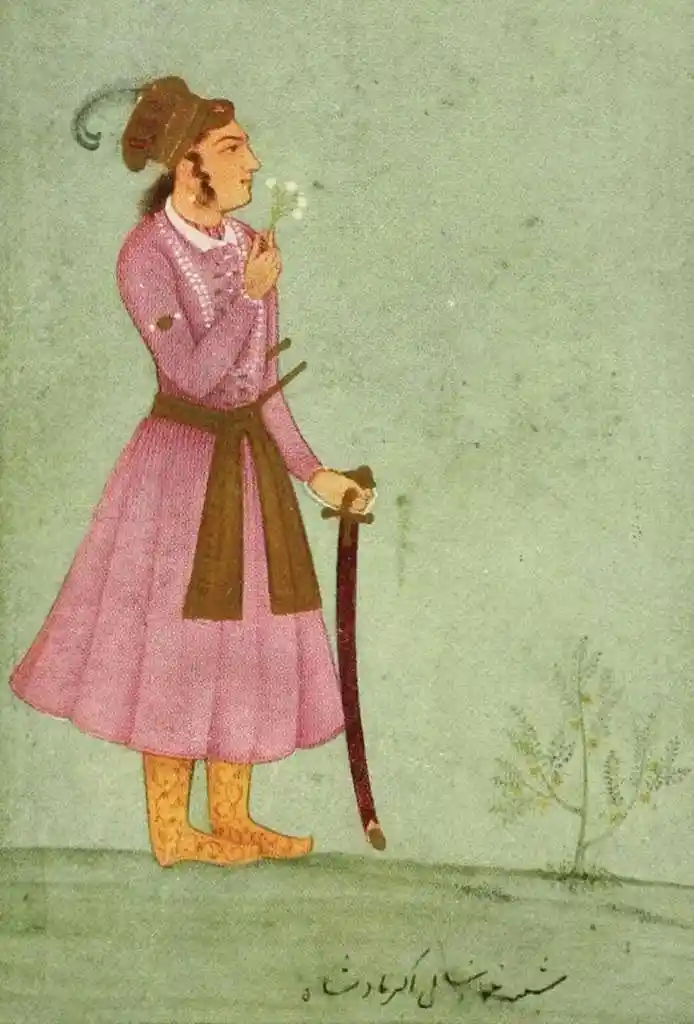
साथ ही मुग़ल काल में हर बात को लिखने की परम्परा थी और इनका समय भी ज्यादा पुराना नहीं है इसलिए इनके नवरत्नों और उनके समय को लेकर अधिकतर इतिहासकार एकमत हैं। इनके दरबार के नवरत्न इस प्रकार थे।
1. बीरबल
1528 ई. में काल्पी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला बीरबल अकबर का सर्वप्रिय एवं सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र था। उसका बचपन का नाम महेश दास था। अपनी हाजिर-जवाबी, चतुराई एवं स्वामिभक्ति के कारण अकबर के वह बहुत करीब था। उसे ‘कविराज’ की उपाधि प्राप्त थी।
अकबर ने उसे राजा की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर ने उसे 2000 मनसब से भी नवाजा था। उसे नगरकोट, कांगड़ा, कालिंजर में जागीरें भी प्रदान की गईं। अकबर के प्रिय पात्र होने के कारण बीरबल से अन्य दरबारी ईर्ष्या करते थे।
अकबर ने सीकरी के किले में बीरबल के लिए एक भव्य महल का निर्माण भी करवाया था, जो आज भी विद्यमान है। बीरबल अपने चुटकुलों के लिए अति प्रसिद्ध है।
1583 ई. में अकबर ने उसे न्यायविभाग का उच्चाधिकारी नियुक्त किया। वह प्रार्थना-पत्र जांच कर स्वीकार करता था तथा प्रार्थी को सम्राट् के समक्ष पेश करता था।
1586 ई. में यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय आध्यात्मिक मित्र की मृत्यु ने अकबर को उदासीन कर दिया। दो दिन और दो रातें उसने उपवास किया और उसे सांसारिक वस्तुओं से घृणा हो गई। अकबर के जीवन पर हिंदू धर्म का प्रभाव बीरबल के कारण ही पड़ा।
2. टोडरमल
उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय वंश में उत्पन्न टोडरमल ने आरंभ में शेरशाह सूरी के पास काम किया। सूर वंश के पतन के पश्चात् उसने अकबर की सेना में नौकरी शुरू कर दी। 1562 ई. में प्रमुख अधिकारी बना।
1572 ई. में अकबर ने उसे गुजरात प्रदेश का दीवान नियुक्त किया। 1582 ई. में वह प्रधानमंत्री बना। उसे ‘दीवान-ए-अशरफ’ का पद प्रदान किया गया। टोडरमल ने भूमि संबंधी अनेक सुधार कार्य किए। अकबर का नवरत्न होते हुए भी उसने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा।
वह निर्भीक, साहसी एवं लोभरहित था। वह बुद्धिमान होने के साथ-साथ एक कुशल सैनिक भी था। उसे अनेक राज्यों में राजदूत बनाकर भेजा। टोडरमल हिंदू धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने अकबर के ‘दीन-ए-इलाही’ धर्म को नहीं अपनाया। इस वीर और साहसी विद्वान् की मृत्यु 1589 ई. में हो गई।
3. अबुल फजल
अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। उसका जन्म 1550 ई. में सूफी शेख मुबारक के घर में हुआ था। प्रारंभ में उसे बीस सवारों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में 5,000 सवार का मनसबदार नियुक्त हुआ।
अपनी विद्वता एवं कर्तव्यपरायणता के बल पर वह अकबर का सचिव नियुक्त हो गया। वह साहित्य, दर्शनशास्त्र एवं इतिहास का ज्ञाता था। लेखन शैली में उसे अद्भुत कौशल प्राप्त था। वाद-विवाद में बड़े-बड़े विद्वान् उसके समक्ष घुटने टेक देते थे।
मुसलमान होते हुए भी उसे हिंदू धर्मग्रंथों का पूर्ण ज्ञान था। उसे नास्तिक भी कहा जाता था। दीन-ए-इलाही को आरंभ करने की प्रेरणा अकबर को अबुल फजल से ही मिली थी। अबुल फजल की दो रचनाएं ‘अकबरनामा’ तथा ‘आईन-ए-अकबरी’ अति प्रसिद्ध हुई हैं।
‘आईन-ए-अकबरी’ तीन भागों में रचित है तथा अकबर के काल की समस्त जानकारी इसमें मिलती है। अबुल फजल एक सफल योद्धा भी था। लेकिन अकबर के बेटे सलीम के इशारे पर बुंदेल सरदार ने उसकी हत्या कर दी।
1602 ई. में इस हत्या के पश्चात् अकबर ने अत्यंत दुःखी होकर कहा था कि ‘अगर सलीम मुझसे नाराज था तो उसे मुझे मार देना चाहिए था, न कि मेरे मित्र को।’ अकबर अपने प्रिय मित्र अबुल फजल की मृत्यु से इतना दुःखी हो गया कि कुछ काल पश्चात् उसकी भी मृत्यु हो गई।
4. भगवानदास
आमेर के राजा भारमल का बेटा राजा भगवानदास भी अकबर के नवरत्नों में था। राजा भगवानदास की बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। 1562 ई. से 1589 ई. तक वह अकबर का मित्र रहा। गुजरात से काबुल और कश्मीर तक उसने बहुत से युद्धों में भाग लिया।
योग्यता और कर्तव्यपरायणता के कारण उसे 5,000 का मनसबदार बना दिया गया। उसे ‘अमीर उल-उमरा’ की उपाधि दी गई। वह केवल प्रधानमंत्री के अधीन था। वह कुछ समय के लिए लाहौर का गवर्नर भी रहा।
टोडरमल, कुलिज खां और भगवानदास अकबर की अनुपस्थिति के समय केंद्रीय शासन के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। भगवानदास की मृत्यु के अवसर पर अकबर को इतना अधिक दुःख पहुंचा कि उसने उसके पुत्र मानसिंह को अफसोस का पत्र लिखा और सलीम को अपना दुःख प्रकट करने के लिए भेजा और उसके स्थान पर मानसिंह को नवरत्नों में जगह दी।
अकबर के मुख्य सेनापति तथा उसके साम्राज्य को विशाल बनानेवालों में राजा मानसिंह का नाम सर्वप्रथम आता है। मानसिंह के संपर्क में आकर ही अकबर ने हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को बंद करवा दिया तथा जजिया जैसे घृणित कर को हटा दिया।
मानसिंह के कारण ही अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध सफलता मिली थी। काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों को विजय करने का मुख्य श्रेय मानसिंह को ही है। अतः अकबर मानसिंह को अपने दरबार के अन्य नवरत्नों की तरह एक सम्मान की दृष्टि से देखता था।
5. तानसेन
संगीत सम्राट् तानसेन अपने संगीत के कारण अकबर के दरबार का महत्त्वपूर्ण रत्न था। उसका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट् ने उसे अपने दरबार में बुलाया था।
अबुल फजल ने तानसेन के विषय में लिखा है कि भारत में एक सहस्र वर्ष से इतना अच्छा गायक नहीं हुआ है। उसने नवीन रागों का निर्माण किया। वह स्वयं कविता एवं गीत भी लिखता था। तानसेन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था।
6. अब्दुर्रहीम खानखाना
अब्दुर्रहीम, अकबर के सरक्षंक बैरम खां का पुत्र था। बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चल बसे। कुछ लोगो का मानना है कि अकबर ने ही बैरम खान को मरवा दिया था। अतः अब्दुर्रहीम का पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा स्वयं अकबर ने की थी।
पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। रहीम एक उच्च कोटि के विद्वान् एवं कवि थे। उन्होंने ‘बाबरनामा’ का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था।
रहीम जहांगीर के गुरु थे। इनके द्वारा ही जहांगीर कविता एवं चित्रकला का अत्यधिक प्रेमी हो गया था। रहीम एक विद्वान् ही नहीं, बल्कि वीर सेनानायक भी थे। उन्होंने गुजरात के शासक को पराजित किया था, जिसके कारण अकबर ने इन्हें ‘खानखाना’ उपाधि से विभूषित किया था।
7. मुल्ला दो प्याजा
मुल्ला दो प्याजा अरब निवासी था। वह हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। मुल्ला दो प्याजा एक बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपनी बुद्धिमत्ता एवं वाक्पटुता के कारण वह सम्राट् का कृपापात्र बन गया और सम्राट् ने उसे नवरत्नों में स्थान दिया। इनको दो प्याजा भोजन अत्यधिक प्रिय लगता था, इसलिए सम्राट् ने इनको ‘दो प्याजा’ की उपाधि से विभूषित किया।
8. हकीम हुमाम
हकीम हुमाम अकबर के रसोईघर का प्रधान था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी से बादशाह अत्यधिक प्रभावित थे तथा राजदरबार में उसने उसे अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया था।
9. फैजी
अकबर के दरबार का अंतिम नवरत्न फैजी को कहा जा सकता है। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। वह एक विद्वान् एवं उदार विचारों का व्यक्ति था। उसको अकबर ने राजकवि के पद पर आसीन किया था।
फैजी ने भी ‘अकबरनामा’ नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। अकबर द्वारा चलाए गए ‘दीन-ए-इलाही’ का फैजी भी समर्थक था। 1595 ई. में उसकी मृत्यु हो गई।
निष्कर्ष
अकबर ने अपनी महानता के अनुरूप ही अपने दरबार में योग्य, विद्वान् एवं महान् व्यक्तियों को स्थान दिया और यही कारण है कि अकबर भारत में एक विशाल, व्यवस्थित, समृद्ध तथा स्थायी साम्राज्य का निर्माण करने में सफल रहा।
अकबर प्रतिभा का आदर करनेवाला व्यक्ति था तथा अपने नवरत्नों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। अकबर के सद्व्यवहार के कारण इन नवरत्नों का पूर्ण सहयोग उसे प्राप्त था। उसके दरबार की शान में इन नवरत्नों ने चार-चांद लगा दिए थे।
इस्लाम धर्म का उदय कैसे और कहाँ से हुआ पढ़ने के लिए क्लिक करें



